कैलाश बृजवासी
तब . . .
". . . कि संस्कृत पढ़ाने वाली अध्यापिका का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था और वे व्यवहार भी स्नेह भरा रखती थीं। उन दिनों हमें संस्कृत या उर्दू में से कोई एक विषय लेना होता था। अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव देखिए- उर्दू विषय बहुत कम लोग लिया करते थे. . ."
जुलाई 1973
मैं उस समय ठीक दस बरस का था किन्तु मुझे अच्छी तरह से याद है कि शुरूआत में मुझे यहां का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। जिस स्कूल से मैं आया था वहां कड़ा अनुशासन था फिर पढ़ाने वाली सभी ‘सिस्टर्स’ ही थीं। मुझे पहली बार पता चला कि आम व्यक्ति (साड़ी पहनने वाली मैडम या शर्ट, पेंट और धोती पहनने वाल सर) भी पढ़ाने का काम कर सकते हैं।


कक्षा-5 (जूनियर स्कूल) में मैंने प्रवेश लिया था। इतना बड़ा स्कूल देखकर ही ताज्जुब होता था। स्कूल बस कक्षा से बहुत दूर रूका करती थी। वहां से दूर लड़कों के साथ चलकर अपनी कक्षा तक जाना और दिनभर बैठकर छुट्टी होने का इंतजार करना, शायद कभी न भूल पाऊंगा। एक पीरियड के खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे बाहर भाग जाते और दूसरे अध्यापक के आने का इन्तजार करते तब मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहता था। इससे पहले वाले स्कूल में मैंने यही सीखा था। समय पर पानी पीना, समय पर बाहर जाना आदि आदि। यहां कक्षा में होने वाल शोर को सुनकर ही घबराहट होती थी। बच्चे खूब शोर मचाया करते थे।
कैसे अध्यापक, कैसा व्यवहार?
एक बात और, जो मुझे उन दिनों बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, वो यह कि हर विषय अलग-अलग अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता था। इससे पहले मैं कक्षा चार तक जिस माहौल में पढ़ा उसमें एक ही अध्यापिका सभी विषय पढ़ाया करती थी। इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव – जो मैंने महसूस किया- ये पड़ा कि जहां पहले सभी विषयों से मेरा समान रूप से जुडाव रहा करता था, वहीं अब मुझे केवल वे ही विषय ज़्यादा आने लगे जिनके अध्यापक अपने व्यवहार से मूझे प्रभावित करते थे। बात कुछ अजीब-सी ज़रूर है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव मेरे ‘केरियर’ पर पड़ा (कम से कम मैं आज तक ऐसा मानता हूं)।
मज़ेदारी बात तो यह है कि इस विद्यालय में उन दिनों विज्ञान कक्ष अलग से हुआ करता था और विज्ञान की कक्षाएं वहीं लगा करती थी। ये पीरियड अक्सर खाली रहा करता था। (खाली पीरियड की अवधारणा भी मैंने इसी स्कूल में जानी)। सो इस पीरियड के दौरान हम एक बड़ के पेड़ के नीचे खेला करते थे। ऐेसे में जब कभी विज्ञान के अध्यापक कक्षा लिया करते तो हमें बड़ी कोफ्त होती थी क्योंकि हमारा मूड तो खेल का हुआ करता था।
हमारे चित्रकला के अध्यापक ने अपनी कक्षा में हमसे कहा, ‘’उस ओर कागज़ रखे हैं और इस तरु रंग, उठाओं और जितने चाहो चित्र बताओं।‘’ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चित्रकला विषय से उसी दिन से मेरा नाता बहुत गहराई से जुड़ गया। भावनाओं क अभिव्यक्ति का इतना सरल-सा अवसर अन्य किसी भी विषय में मुझे नज़र नहीं आ सका।
सामाजिक ज्ञान के अध्यापक हो एक बार मेरे द्वारा बनाया गया पृथ्वी और सूरज का चित्र इतना भद्दा और खराब लगा कि पूरी कक्षा के सामने उन्होंने मेरी कॉपी मेरे मुंह पर फेंक दी। इस घटना के बाद बहुत दिनो तक मैं स्कूल नहीं गया। जब गया तब भी उन अध्यापक से नज़रें न मिला सका। हद तो ये थी कि बस्ते से सामाजिक ज्ञान की किताब निकालते और रखते हुए भी मुझे डर-सा लगता था। आप शायद ही विश्वास करें किन्तु इस घटना के बाद मैं आठ वर्ष तक इसी विद्यालय में रहा और कई बार इन अध्यापक से मेरा आमना-सामना हुआ किन्तु नमस्ते करना तो दूर, उन्हें देखकर मैं अपनी राह तक बदल लिया करता था।
हर रोज़ सुबह प्रार्थना से पहले झण्डारोहण कार्यक्रम हुआ करता था। कार्यक्रम मे कुछ व्यायाम और कभी-कभी सफाई निरीक्षण का भी काम होता था। कक्षा छह की बात है। एक दिन हिन्दी के अध्यापक ने मेरे बाल बड़े होने की वजह से मुझे लाइन से पकड़ कर मुझे बुरी तरह झिझोड़ दिया। ऐसी बात नहीं थीं कि लाइन में से केवल मुझे ही निकाला गया था, चार-पांच और लड़कों को भी बाल बड़े होने की वजह से ही निकाला गया था। लेकिन सज़ा के लिये सिर्फ मुझे ही चुना जाना और अपशब्द कहना, उस अध्यापक को मुझ से बहुत दूर ले गया।
सभी विषयो में शायद ‘संस्कृत’ विषयों ही एकमात्र ऐसा विषय था जिसकी सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाई जाती थी। सभी बच्चे काफी व्यंगात्मक शैली में संस्कृत के वाक्य बोला करते थे लेकिन इसी विषय की कक्षा में बैठने में बड़ा मज़ा आता था। कारण सीधा-सा था कि संस्कृत पढ़ाने वाली अध्यापिका का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था और वे व्यवहार भी स्नेह भरा रखतीं थी। उन दिनों हमें संस्कृत या उर्दू में से कोई एक विषय लेना होता था। अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव देखिए –उर्दू विषय बहुत कम लोग लिया करते थे क्योंकि उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापक काफी बुजुर्ग और गुस्सैल थे। लड़के आपस में बात किया करते थे कि यदि संस्कृत वाली अध्यापिका ही उर्दू पढ़ाएं तब हमें उर्दू लेकर पढ़ने में मज़ा आएगा।
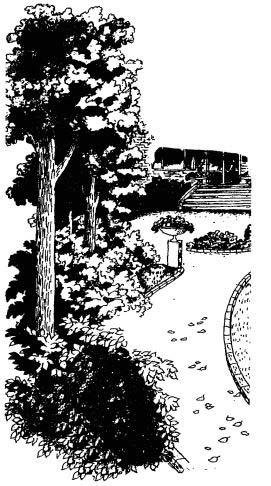 मुझे उन दिनो दो कालांशों (पीरियड) का खासतौर पर इंतजार रहा करता था। एक ‘भोजनावकाश’ (डेढ़ घंटे का) और दूसरा ‘खेल’। भोजनावकाश में भी हम लोग तरह-तरह के खेल खेला करते थे, लेकिन दोनों ही सत्रों में काफी अन्तर होता था। शाम को खिलाए जाने वाले खेलों में हमें फुटबाल, हॉकी, बास्केट बॉल आदि में से किसी एक ही खेल को चुन कर पूरे साल वही खेलना पड़ता था। चाह कर भी दूसरा खेल नहीं खेल सकते थे। ये भड़ास हम भोजनावकाश में अपने पसंदीदा खेल खेल कर निकाल लिया करते थे। अब तक हम यही सुनते आए थे कि जो खेल खिलाने वाल सर (पी.टी.आई.) होते हैं वे काफी सख्त व्यवहार वाले होते हैं। उनका नाम सुनते ही डर लगना चाहिए आदि-आदि। खेलों के सत्र का कड़े अनुशासन के साथ संचालन करने के बावजूद भी ये सर सभी को इतने अच्छे क्यों लगते रहे शयद इस पर शोध की आवश्यकता हो – लेकिन जहां तक मैंने उन्हें जाना, एक प्रकार की आवश्यक दूरी बनाए रखने के साथ ही बच्चों के प्रति खेल खिलाते समय झलकने वाली आत्मीयता इसका कारण हो। पता नहीं ...... शायद।
मुझे उन दिनो दो कालांशों (पीरियड) का खासतौर पर इंतजार रहा करता था। एक ‘भोजनावकाश’ (डेढ़ घंटे का) और दूसरा ‘खेल’। भोजनावकाश में भी हम लोग तरह-तरह के खेल खेला करते थे, लेकिन दोनों ही सत्रों में काफी अन्तर होता था। शाम को खिलाए जाने वाले खेलों में हमें फुटबाल, हॉकी, बास्केट बॉल आदि में से किसी एक ही खेल को चुन कर पूरे साल वही खेलना पड़ता था। चाह कर भी दूसरा खेल नहीं खेल सकते थे। ये भड़ास हम भोजनावकाश में अपने पसंदीदा खेल खेल कर निकाल लिया करते थे। अब तक हम यही सुनते आए थे कि जो खेल खिलाने वाल सर (पी.टी.आई.) होते हैं वे काफी सख्त व्यवहार वाले होते हैं। उनका नाम सुनते ही डर लगना चाहिए आदि-आदि। खेलों के सत्र का कड़े अनुशासन के साथ संचालन करने के बावजूद भी ये सर सभी को इतने अच्छे क्यों लगते रहे शयद इस पर शोध की आवश्यकता हो – लेकिन जहां तक मैंने उन्हें जाना, एक प्रकार की आवश्यक दूरी बनाए रखने के साथ ही बच्चों के प्रति खेल खिलाते समय झलकने वाली आत्मीयता इसका कारण हो। पता नहीं ...... शायद।
छटवीं कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका ने पहले ही दिन से जो डर मन मे बिठाया था वो शायद आज तक कायम है। ‘’मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। मुझे मेरी कक्षा में बिल्कुल भी आवाज पसन्द नहीं है। जब तक मैं कक्षा में पढ़ाऊं तब तक कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, वरना मैं उसे तुरन्त कक्षा से बाहर निकाल दूंगी।‘’ उनके ऐसे वाक्य मुझे अब तक याद हैं। अपने पास बैठे लड़के से पेंसिल कटर मांगने की वजह से उन्होंने मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया और पूरे सप्ताह अपनी कक्षा में अन्दर नही आने दिया, ये घटना मुझे हिला देने वाली थी। पूरा सप्ताह अपनी कक्षा के सामने बाहर की ओर लगे दरवाजे की चौखट पर खेड़े रहकर बिताना, भूलने जैसी बात भी तो नहीं है। कक्षा-10 तक वही अध्यापिका हमें पढ़ाती रही। किन्तु उनके द्वारा पढ़ाए जाने के कारण विज्ञान और बाद में रसायन शास्त्र मानों मेरे शत्रु ही बन गए।
जरा विरोधाभास देखिए, उसी कक्षा में (कक्षा-6) उन दिनों एक नई अध्यापिका आईं और उन्होंने हमें अंग्रेजी और चित्रकला दोनों ही विषय पढ़ाना शुरू किया। पहल ही दिन उन्होंने कहा, ‘’आप लोग इतने खामोश क्यों बैठे हैं? मुझे ऐसी कक्षा अच्छी नहीं लगती। मैं भी बात करूंगी और आप भी बात करेंगे तब कक्षा में खूब मज़ा आएगा।‘’
आप यकीन मानिए दिनभर हमें केवल उन्हीं अध्यापिका की कक्षा का इंतजार रहा करता था। केवल दो या तीन प्रिय छात्र या छात्राएं नहीं बल्कि पूरी कक्षा के बच्चों से समान प्यार-व्यवहार को उन दिनों तो मैंने केवल महसूस ही किया था किन्तु आज उसका महत्व भी जान लिया हे। लगभग यही बात मैं हिन्दी ओर सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका के विषय में भी कहूंगा। उन्होंने एक दिन कहा, ‘’यदि तारीखों और सन् की वजह से आपको इतिहास कठिन लगता है तो आप उन्हें नज़र अंदाज़ कर के पढ़ें। तारीख याद रखे बिना इतिहास पढ़ें, उसकी घटनाएं पढ़ें, कहानी की तरह। मैं परीक्षाओं में भी तारीखें न लिखने की वजह से अंक नहीं काटूंगी।‘’
शायद ये छोटी-सी कीमती बात हमारे लिए कठिन इतिहास को सरल बना गई। इतिहास से मैंने अपना नाता स्नातक स्तर तक बनाए रखा।
 उन दिनों कक्षा नौ से ही हमें अपने लिए विशेष लेने होते थे जो कि विज्ञान- गणित, विज्ञान- जीव विज्ञान और कला थे। एक बार लगा, चला कठिन विषयों से पीछा छूटा। किन्तु विडम्बना देखिए। न चाहते हुए भी मुझे ‘विज्ञान-गणित’ विषय ही लेना पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर वाल मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, या उनका कोई दबाव था मुझ पर विषय चयन को लेकर। इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब रहा जो बचपन से ही मेरे माता-पिता ने मुझे अपने निर्णयों से ही सीखने की आदत डाली।
उन दिनों कक्षा नौ से ही हमें अपने लिए विशेष लेने होते थे जो कि विज्ञान- गणित, विज्ञान- जीव विज्ञान और कला थे। एक बार लगा, चला कठिन विषयों से पीछा छूटा। किन्तु विडम्बना देखिए। न चाहते हुए भी मुझे ‘विज्ञान-गणित’ विषय ही लेना पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि मेरे घर वाल मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, या उनका कोई दबाव था मुझ पर विषय चयन को लेकर। इस मामले में मैं बड़ा खुशनसीब रहा जो बचपन से ही मेरे माता-पिता ने मुझे अपने निर्णयों से ही सीखने की आदत डाली।
वास्तव मे जब मैंने देखा कि हमारी पूरी कक्षा ‘विज्ञान-गणित’ विषय ले रही है तो कक्षा के दोस्तों के छूट जाने के मोह ने मुझे उधर धकेल दिया। कक्षा में जब देखा कि पिछले तीन सालों से विज्ञान पढ़ाने वाली अध्यापिका ही अब रसायन शास्त्र भी पढ़ाएंगी तब मुझे ये दोनों विषय समान रूप से कठिनतम लेने लगे। पहली बार जगब रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के दर्शन किये, तब हमें ‘लैब’ में हो सकने वाली दुघर्टनाओं और खतरों के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी गई कि सभी उपकरण खौफनाक लगने लगे। दो-दो के जोड़ो में प्रयोग करते समय भी परखनली में ‘केमिकल्स’ डालते हुए डर ही ज़्यादा लगता। यदि कुछ अच्छा लगता तो वो था अपनी फाईल में प्रयोग से संबंधित चित्रों को बनाना।
सवाल पूछने का मन कई बार किया करता था। किन्तु अध्यापिका के डर से कोई भी एक शब्द तक नहीं पूछ पाता। हम आपस में पूछताछ ज़रूर करते किन्तु प्रयोगशाला से छूटने के बाद। हां, उन दिनों लैब असिसटेन्ट भी नए-नए ही नौकरी पर लगे थे और लैब के परम्परागत तौर-तरीकों को हमारी ही तरह सीखने की प्रक्रिया में चल रहे थे। शायद इसलिए वे हमसे दोस्ताना व्हवहार रखते थे। कई बार हम अपने सवाल उनसे पूछ लिा करते थे। और वे मुस्कुराते हुए जवाब देते – क्या पता यार, मैं भी तो नया-नया आया हूं।
हमारे स्कूल मे भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र की प्रयोगशालाएं बिल्कुल पास-पास थीं। मज़ेदार बात तो यह थी कि जब हमारी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में जाने की बारी आती तो सरल लोलक, परावर्तन के नियम आदि प्रयोग हम खूब मज़े से आपस में चर्चाएं करते हुए किया करते। कारण इस विषय के अध्यापक का मस्त–मौला स्वभाव था। वे अपनी ही मस्ती में मगन रहते हुए पढ़ाते और हमें भी मस्ती से काम करने देते।
बहुत-सी बार तो इतनी आवाज़ होती कि पास की लैब से रसायन शास्त्र की अध्यापिका को आ कर कहना पड़ता कि आप लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं। ये लेबोरेटरी है, ज़रा मेरी लैब मे चल रह देखिए बच्चे कितनी शान्ति से अपना काम कर रहे हैं। कुछ देर तो हम चुप हो जाते। जब वो चली जाती तो मुड़कर अपने भौतिक शास्त्र के अध्यापक की ओर देखते। उनको मुस्कुराता हुआ पा कर खुद भी खिलखिला उठते। उस समय वे हमें बनाबटी आंखें दिखाते और श... श.... श.....श..... का इशारा करने लगते। ये बात सन् 1979 की है।
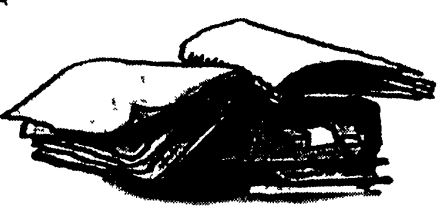 यदि गणित की बात करूं तो न तो अध्यापक और न ही विषय मुझे कभी अच्छा लगा। कक्षा दस तक पांच वर्ष के दौरान लगभग सात अध्यापकों ने इसे अपने-अपने तरीके से हमें पढ़ाने की कोशिश की। हर बार मेरे सबसे कम अंक इसी विषय मे आते। कक्षा सात में तो एक दिन जब गणित के अध्यापक बोर्ड पर सवाल कर रहे थे तो मुझे नींद ही आ गई। आंख खुली तो अध्यापक ठीक मेरी मेज़ के सामने खड़े थे और पूरी कक्षा हंस रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर आ कर कहा, ‘’हम दोनों ही एक बार दौड़ लगाते हैं मुझे भी नींद आ रही है।‘’ हालांकि दौड़ तो हम लोगों ने नहीं लगाई लेकिन उनके दोस्ताना व्यवहार ने मुझे भयभीत नहीं होने दिया। बदकिस्मती ही कहूंगा जो वे अध्यापक केवल छह माह तक ही विद्यालय में रहे।
यदि गणित की बात करूं तो न तो अध्यापक और न ही विषय मुझे कभी अच्छा लगा। कक्षा दस तक पांच वर्ष के दौरान लगभग सात अध्यापकों ने इसे अपने-अपने तरीके से हमें पढ़ाने की कोशिश की। हर बार मेरे सबसे कम अंक इसी विषय मे आते। कक्षा सात में तो एक दिन जब गणित के अध्यापक बोर्ड पर सवाल कर रहे थे तो मुझे नींद ही आ गई। आंख खुली तो अध्यापक ठीक मेरी मेज़ के सामने खड़े थे और पूरी कक्षा हंस रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर आ कर कहा, ‘’हम दोनों ही एक बार दौड़ लगाते हैं मुझे भी नींद आ रही है।‘’ हालांकि दौड़ तो हम लोगों ने नहीं लगाई लेकिन उनके दोस्ताना व्यवहार ने मुझे भयभीत नहीं होने दिया। बदकिस्मती ही कहूंगा जो वे अध्यापक केवल छह माह तक ही विद्यालय में रहे।
हमारी हिन्दी की अध्यापिका काफी भावुक थी। हिन्दी विषय शायद शुरू से आखिर तक (कक्षा 11 तक) सबसे आसान विषय (दूसरे विषयों की तुलना में) समझा जाता था। अध्यापिका की आवाज़ बहुत धीमी थी और वे अन्तिम दो पंक्तियों मे बैठे साथियों तक नहीं पहुंच पाती थी। आगे जो अनुभव लिखने जा रहा हूं उसके बाद ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि ‘’जो भोला, सीधा-सादा और अपने काम से मतलब रखने वाला होता है उसे अन्य लोग ज़रूर तंग करते हैं’’ हुआ यूं एक दिन कुछ लड़कों ने मिलकर प्रिंसिपल साहब के पास जा कर शिकायत कर दी कि हमें हिन्दी की अध्यापिका जो भी पढ़ाती हैं वो समझ में नहीं आता है, उनकी आवाज भी बहुत धीमी है, वो काफी धीरे-धीरे बोलती हैं, कक्षा में पाठ के प्रश्न–उत्तरों को हल नहीं करवाती, आदि-आदि। इसके अगले ही दिन जब वे कक्षा में आईं तो काफी गंभीर थीं। उन्होंने काफी शान्तिपूर्ण माहौल में एक पाठ पढ़ाया और अन्त में पूछा ‘’क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया?
--"जी मैडम’’ सभी ने उत्तर दिया।
--"क्या मेरी आवाज़ भी सभी लोगों को सुनाई दी?"
-- "जी, हां मैडम।"
-- "त ........ तो फिर ये ............" कहते-कहते वे बुरी तरह से रो पड़ीं।
उनका कहना था कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया। लेकिन मुझसे सम्बन्धित होने के कारण यदि ये पहले सीधे मुझे ही बताई जाती तो मैं अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करने की कोशिश करती। आप लोगों ने तो सीधे ही प्रिंसिपल साहब से बात कर ली। आप लोगों को पता है कि ये मेरे लिए कितने अपमान की बात है?
हम सभी लोग एकदम शान्ति और अचरज से उन्हें देखे जा रहे थे। किसी अध्यापिका को कक्षा में इस तरह रोते हुए देखना वाकई ऐसी बात थी जिसने बहुत गइराई से मुझे यह समझाया कि ये ठीक नहीं हुआ। मैडम का कहना सही था। कक्षा-10 की बात थी, सन् 1980 की।
कैलाश बृजवासी – विद्या भवन, उदयपुर के शिक्षा केन्द्र में कार्यरत। बच्चों के साथ काम का व्यापक अनुभव।
उलटते-पलटते ध्रुव
 पृथवी के चुंबकीय ध्रुव उलटते-पलटते रहते हैं, यानी आज जहां उत्तर ध्रुव है कभी वहां दक्षिणी ध्रुव रहा होगा और दक्षिणी ध्रुव की जगह उत्तरी ध्रुव। लेकिन ऐसी किसी पलटन के वक्त चुंबकीय ध्रुव अपनी नई स्थिति में तुरंत स्थिर नहीं हो जाते बल्कि शुरूआती वर्षो में काफी तेजी से इधर-उधर घूमते रहते हैं। डेढ़ करोड़ साल पहले हुई ऐसी ही एक पलटन के समय उत्तरी ध्रुव की बदलती स्थितियां। इस दौरान स्थिर होने से पहले करीब एक हजार साल उत्तरी ध्रुव यहां-वहां घूमता रहा था।
पृथवी के चुंबकीय ध्रुव उलटते-पलटते रहते हैं, यानी आज जहां उत्तर ध्रुव है कभी वहां दक्षिणी ध्रुव रहा होगा और दक्षिणी ध्रुव की जगह उत्तरी ध्रुव। लेकिन ऐसी किसी पलटन के वक्त चुंबकीय ध्रुव अपनी नई स्थिति में तुरंत स्थिर नहीं हो जाते बल्कि शुरूआती वर्षो में काफी तेजी से इधर-उधर घूमते रहते हैं। डेढ़ करोड़ साल पहले हुई ऐसी ही एक पलटन के समय उत्तरी ध्रुव की बदलती स्थितियां। इस दौरान स्थिर होने से पहले करीब एक हजार साल उत्तरी ध्रुव यहां-वहां घूमता रहा था।

