अनुपम मिश्र पिछले दो दिनों में हमें तीनों संस्थाओं को देखने का सुअवसर मिला। सच कहा जाए तो यहां आने से पहले इनके नाम तक से भी ठीक परिचय न था, न विज्ञान से ही ज्यादा संबंध था। लेकिन इन तीन दिनों में, एक तरह से, विज्ञान की तीन मूर्तियों का दर्शन हमें हो सका। सूक्ष्म संसार कितना विराट हो सकता है, वो हमने पहली संस्था में देखा। ‘सेल' तक का नाम ही सुना था, लेकिन उसके भी कितने टुकड़े हो सकते हैं, उन पर कितना काम किया जा सकता है, उसकी थोड़ी-सी झलक देखी। बचपन में धरती वाले पाठ में पढ़ते थे कि हमारी धरती ‘रत्नगर्भा' है। दुसरी संस्था में इस शब्द का सही अर्थ समझने का अवसर मिला। पता लगा कि आप लोग कितने ही रत्न खोजने में लगे हैं और धरती की परत-परत खोल रहे हैं। तीसरी संस्था में रस को लेकर काम चल रहा है। मैं सोचता हूं हमारा सारा जीवन ही रसमय है। तो इन तीनों विलक्षण संस्थाओं को, इन दो-तीन दिनों में पास से देखने का मौका मिला।
पिछले दो दिनों में हमें तीनों संस्थाओं को देखने का सुअवसर मिला। सच कहा जाए तो यहां आने से पहले इनके नाम तक से भी ठीक परिचय न था, न विज्ञान से ही ज्यादा संबंध था। लेकिन इन तीन दिनों में, एक तरह से, विज्ञान की तीन मूर्तियों का दर्शन हमें हो सका। सूक्ष्म संसार कितना विराट हो सकता है, वो हमने पहली संस्था में देखा। ‘सेल' तक का नाम ही सुना था, लेकिन उसके भी कितने टुकड़े हो सकते हैं, उन पर कितना काम किया जा सकता है, उसकी थोड़ी-सी झलक देखी। बचपन में धरती वाले पाठ में पढ़ते थे कि हमारी धरती ‘रत्नगर्भा' है। दुसरी संस्था में इस शब्द का सही अर्थ समझने का अवसर मिला। पता लगा कि आप लोग कितने ही रत्न खोजने में लगे हैं और धरती की परत-परत खोल रहे हैं। तीसरी संस्था में रस को लेकर काम चल रहा है। मैं सोचता हूं हमारा सारा जीवन ही रसमय है। तो इन तीनों विलक्षण संस्थाओं को, इन दो-तीन दिनों में पास से देखने का मौका मिला।
जैसा कि मेरे वरिष्ठ साथियों ने भी कहा था शोध एक प्रकार का तप है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस तप का फल आप अकेले अपने साथ ले जाएंगे। आप इसके फल को समाज में, समाज की भलाई के लिए बांट देते हैं। कल जब हमें एक संस्था का परिचय दिया जा रहा था तो उसके तीन उद्देश्य बताए गए थे। उसमें ‘ज्ञान और शोध' एक था, दूसरा ‘अर्थ’ और तीसरा 'समाज'। फिर उन्होंने कहा आजकल ‘अर्थ’ का ज़माना है, उसका बोलबाला है, इसलिए सबसे प्रथम हम अर्थ के बारे में ही कुछ समझते हैं। मुझे यह भी लगता है कि हमारे समाज में भी कभी ‘अर्थ’ को भूल कर कोई काम किया हो, ऐसा नहीं। हमारे यहां अर्थ को देवी से जोड़ते हैं और वह देवी भी आप सबके सामने है, हमने उन्हें ‘महालक्ष्मी' कहा है। महालक्ष्मी का परिवार जब हमारे तपस्वियों या मनीषियों ने बनाया होगा, उन्हें विष्णु से जोड़ा जो विवेक के देवता हैं। तो ‘अर्थ’ का होना कोई बुरा नहीं लेकिन अर्थ के लिए विवेक खोना बुरा है। आप देखेंगे उन एशिया के देशों को जिन्हें दो-चार महीने पहले तक ‘एशियन टाइगर' कहा जाता था, उनकी अर्थव्यवस्था छलांग लगाकर हम जैसे देशों से आगे निकली थी, आज उन्हें आप भरभराकर गिरते भी देख रहे हैं पिछले एक-दो महीनों में। तो यह अर्थ वाले मामले में हमें विवेक का ध्यान रखना ही चाहिए।
जो कुछ काम हम लोगों ने इन दो-तीन दिनों में देखा उनमें से कुछ माथी मरुभूमि के 50 सेंटीग्रेड तापमान में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ, मैं गलत नहीं हूं तो -50" (शून्य से 50" नीचे) सेंटीग्रेड तापमान में, एंटार्कटिक में जो कुछ कर रहे हैं, उसके प्रयोग भी दिखाए गए। ये बिल्कुल दो अलग-अलग छोर हैं।
फिर कोई वैज्ञानिक रेशम के धागे को मजबूत बनाने में लगे हैं तो दूसरी ओर जो सबसे मज़बूत अपराधी माना जाता है, उसको डी. एन. ए. के जरिए कमजोर कैसे साबित किया जा सकता है यह भी देखा। एक छोर से दूसरे छोर तक का काम आप सब लोगों ने इतने प्रेम और लगन के साथ दिखाया है कि उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने व धन्यवाद कहने के लिए ही मैं यहां खड़ा हुआ हूं।
भाषावाली बात आई - हम लोगों को यह प्रयोग बताया गया ‘समागम'। हिन्दी में लिखने, पढ़ने की बात। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मुझे इस समागम में जो कुछ मिला, वह मैंने देखा कि ‘मन की भाषा' है। आप लोगों ने कैसी बारीक-बारीक चीज़ों को मन से इतने प्रेम से हम जैसे लोगों को समझाने की कोशिश की है, बिना यह देखे कि हमारी पात्रता क्या है। कम-से-कम मैं अपने बारे में कहूंगा कि कल जब हमें सोना निकालने वाले प्रयोग में बताया गया है कि एक टन मिट्टी में दशमलव शून्य पांच ग्राम सोना भी निकल आए तो ठीक है, मैं उस दर्ज में भी नहीं हूं। फिर भी अपने अपने यंत्रों में लगाकर देख लिया कि, भई चलो, एक टन मिट्टी में इतना कण बराबर सोना ही सही, उसी तरह हम हैं।
कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं, जिन्हें जल्दी-जल्दी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक साथी हमारे बीच में नहीं हैं, वो वरिष्ठ हैं सिर्फ इस नाते नहीं, लेकिन मुझे कुछ चीजें रिपोर्ट देखकर बहुत आश्चर्यजनक लगीं। प्रो. डी. बाल सुब्रह्मण्यम जिनके एक लेख का जिक्र मैंने एक रिपोर्ट में देखा, उसका शीर्षक देखकर ही बहुत अच्छा लगा कि हमारे एक प्रमुख वैज्ञानिक इस ढंग से लिख सकते हैं। कोई चीज़। बाहर से जिन लोगों को यहां आप बुलाते हैं उसमें मैंने नोम चोमस्की का भी नाम देखा, भाषा पर जिनका अत्याधिक काम रहा है। इन्हीं से मुझे लगा कि कुछ बातें फिर से आपके सामने रखूँ।
18वीं सदी का भारत
हम गुलाम हुए ठीक है, एक दौर आता है दुनिया में कि कुछ लोग जीत का झंडा लेकर निकलते हैं तो कुछ को घुटने टेकने पड़ते हैं मजबूरी में। वह सब दौर खत्म हो गया। लेकिन, उपनिवेश अपना एक असर छोड़ जाता है। जो कोई समाज किसी समाज को हराता है तो उसे तन से भी तोड़ता है। और मन से भी तोड़ता है। यह शायद उसकी मजबूरी भी होती होगी। लेकिन सोचें कि अंग्रेजों के आने से ठीक पहले हमारा देश क्या था। अभी जोशी जी ने जिस काल खंड में आपको खींचने की कोशिश की, वहां अगर आप अभी न आकर बिल्कुल 18वीं शताब्दी की दहलीज पर खड़े होकर अपने देश को देखें। मेरा कहना है कि हमारी कोई भी पाठ्य-पुस्तक, हमारा कोई भी समाज चिंतक, कोई भी राजकीय नेता - सब उस 18वीं शताब्दी के बारे में बिल्कुल शून्य हैं। या तो हम बिल्कुल पीछे की बातें जानते हैं या फिर आज की। 18वीं शताब्दी में हमारे समाज की स्थिति क्या थी? कहां हमने घुटने टेके? उस समय हम क्या थे? इन बातों के बारे में डॉक्युमेंटेशन ढंग से जिन संस्थाओं को, जिन लोगों को करना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं सिर्फ संकेत रूप में एक नाम आपके सामने रखना चाहूंगा। उनका नाम है धर्मपाल जी। इन्होंने इतिहास को बहुत ही भिन्न किस्म से लिखा है। उनकी एक पुस्तक का नाम है ‘साइंस एंड टेकनॉलॉजी इन 18 सेंचुरी, सम कंटेम्पररी एविडेंस' शैली बहुत अच्छी है।
मैं खुद लिखें और वही कहूं कि अठारहवीं शताब्दी में मेरे पास यह था, वह था, रॉकेट था, जहाज़ था तो आप कहेंगे कि यह सब बेवकूफी की बातें हैं। लेकिन धर्मपाल जी की शैली अलग है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी नाम की लंदन में एक लाइब्रेरी है। उसमें अंग्रेजी राज का कुछ लिटरेचर रखा हुआ है। अंग्रेज जब हमारे यहां आए तो कुतूहल के कारण उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठी की। अगर हैदराबाद आए, रायलसीमा गए तो यहां का हल कैसे होता है, कैसे सिंचाई होती है, कैसे फल हैं, यह सब उन्होंने विभिन्न स्तरों, ओहदों में अपने देश को रिपोर्ट के रूप में, कभी-कभी मां-बहन-मित्रों को चिट्ठी के रूप में लिख भेजा था। इस सारे साहित्य को एकत्रित कर वहां सुरक्षित रखा गया। धर्मपाल जी ने अठारह साल उस पुस्तकालय में बैठकर काम किया और ऐसे सारे सबूतों को इकट्ठा किया जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। शायद दो सौ पन्नों में इस तरह की चीजें हैं। और करीब पचास पन्नों में भूमिका, कि यह सब क्या बतलाता है। शायद आपको अचरज होगा सुनकर कि तमिलनाडु के तंजाऊर के एक मंदिर में चेचक फैलने से पहले चेचक का टीका एक पुजारी द्वारा लगाने संबंधी वर्णन किसी एक अंग्रेज़ का मिलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और मुझे लगता है, क्योंकि आप विज्ञान क्षेत्र में हैं, तो ज़रूर इसे अपने ढंग से कभी पलटकर देखें, धर्मपाल जी द्वारा लिखे साहित्य को। केवल पुराना ही सब कुछ अच्छा हो और उससे ही वर्तमान टिका हो, यह नहीं।
मेरे परिचय में कहा गया कि मैंने राजस्थान को पानी दिया है, मैंने पानी नहीं दिया है। राजस्थान समाज ने पानी का जो प्रबंध किया उसका मैंने मुनीम जैसा काम किया, दो किताबों के माध्यम से, जिन्हें आप जैसे लोगों का बहुत प्यार मिला है। मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रखेंगा कि राजस्थान को पानी के मामले में पूरे देश में गरीब प्रांत माना जाता है, जहां 3 से 9 इंच पानी बरसता है। मुझे हैदराबाद का नहीं मालूम, शायद यहां 2530 इंच तो होना ही चाहिए। इसका दसवां हिस्सा पानी जिस जगह को मिले, उसको वर्णन हम लोगों को जब मिला तो हमारी आंखे फटी रही गई। उससे हमारे समाज की चीजों का एक हल्का सा अंदाज़ा लगता है। वहां मरूभूमि में स्कूल शायद सरकार 20 प्रतिशत गांवों तक पहुंचा सकी। डाक घर जिसमें केवल एक लोहे का लाल डिब्बा लगाना है, सिर्फ 28-30 प्रतिशत तक पहुंचाया। अस्पताल 12-15 प्रतिशत, बिजली के बारे में पता चलता है कि सिर्फ 4 प्रतिशत गांवों में पहुंचा पाए हैं। लेकिन जब पानी के बारे में देखा तो पाया यह 99.7 प्रतिशत गांवों में उपलब्ध है। आखिर यह सरकारी आंकड़े थे। हम लोग चौंके कि जहां पानी का बजट प्रकृति ने ही सीमित कर दिया उसके बावजूद 99 प्रतिशत गांवों में पानी है। और डाकघर पहुंचा नहीं पाए, स्कूल पहुंचा नहीं पाए जिसके लिए विश्व बैंक भी उधार देने को तैयार खड़ा है। तो हमें लगा कि इसके पीछे कोई और ताकत है। उस ताकत को देखते यह समझ में आया कि पानी के मामले में उस समय भी इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था; और यह सारा काम सरकार ने नहीं, मरूभूमि में, समाज ने अपने बलबूते पर किया है। अभी शब्दों की बात चली, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अनुवाद के शब्दों से हम काम नहीं चला सकते। बोलियों के साथ हिन्दी का या किसी भी भाषा का जो संपर्क होना चाहिए वह किसी अहं के कारण टूटता है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। राजस्थान की बोलियों में बादल के लिए करीब 40 नाम हमने इकट्ठे किए। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा मिलें, और ये पर्यायवाची नाम नहीं हैं। तो कितना संपन्न समाज रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा वह समाज कि उसने एक-एक बादल को एक-एक ढंग से पकड़ लिया, उसके आकार से, रंग से, उसकी ऊंचाई से, उसके कर्तव्य से। कोई कामचोर बादल हो तो उसका कामचोर बादल नाम रखा होगा, कोई तेज़ रहा हो तो उसका नाम भी तेज़ रखा होगा। इस तरह से सारी चीजें देखते-देखते हमें उस समाज की वैज्ञानिकता का अंदाज़ हो जाता है। आधुनिकतम, जिसको हम वाटर मिशन जैसी संस्थाओं के प्रयोग कहते हैं, ये भी उन गांवों तक पहुंच नहीं पाते हैं। और समाज ने 35,000 गांवों तक पानी पहुंचाने का इतना बड़ा ढांचा खड़ा किया उसको अध्यक्ष कौन? डायरेक्टर कौन? वार्षिक बजट क्या है? आप सर पटक लीजिए आपको पता नहीं चलेगा और एक हजार साल से वह संस्था चल रही है अदृश्य रूप में। तो कहता हूं कि इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा उसका आकार है कि खुद वह निराकार हो गया, आपको दिखाई तक नहीं देता। अन्य संस्थाओं के मुख्यालय हमें देखने को मिलते हैं, उनका लोगो (चिन्ह) दिखता है, उनका अपना झंडा होता है, वार्षिक रिपोर्ट दिखती है। लेकिन मरूभूमि में पानी का इतना विस्तृत इंतजाम करने वाली संस्था के निदेशक तक को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसने काम किया उसका कोई अता-पता नहीं।
अभी शब्दों की बात चली, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अनुवाद के शब्दों से हम काम नहीं चला सकते। बोलियों के साथ हिन्दी का या किसी भी भाषा का जो संपर्क होना चाहिए वह किसी अहं के कारण टूटता है तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। राजस्थान की बोलियों में बादल के लिए करीब 40 नाम हमने इकट्ठे किए। हो सकता है कि उससे भी ज्यादा मिलें, और ये पर्यायवाची नाम नहीं हैं। तो कितना संपन्न समाज रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा वह समाज कि उसने एक-एक बादल को एक-एक ढंग से पकड़ लिया, उसके आकार से, रंग से, उसकी ऊंचाई से, उसके कर्तव्य से। कोई कामचोर बादल हो तो उसका कामचोर बादल नाम रखा होगा, कोई तेज़ रहा हो तो उसका नाम भी तेज़ रखा होगा। इस तरह से सारी चीजें देखते-देखते हमें उस समाज की वैज्ञानिकता का अंदाज़ हो जाता है। आधुनिकतम, जिसको हम वाटर मिशन जैसी संस्थाओं के प्रयोग कहते हैं, ये भी उन गांवों तक पहुंच नहीं पाते हैं। और समाज ने 35,000 गांवों तक पानी पहुंचाने का इतना बड़ा ढांचा खड़ा किया उसको अध्यक्ष कौन? डायरेक्टर कौन? वार्षिक बजट क्या है? आप सर पटक लीजिए आपको पता नहीं चलेगा और एक हजार साल से वह संस्था चल रही है अदृश्य रूप में। तो कहता हूं कि इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा उसका आकार है कि खुद वह निराकार हो गया, आपको दिखाई तक नहीं देता। अन्य संस्थाओं के मुख्यालय हमें देखने को मिलते हैं, उनका लोगो (चिन्ह) दिखता है, उनका अपना झंडा होता है, वार्षिक रिपोर्ट दिखती है। लेकिन मरूभूमि में पानी का इतना विस्तृत इंतजाम करने वाली संस्था के निदेशक तक को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जिसने काम किया उसका कोई अता-पता नहीं।
आम जनता का विज्ञान
एक छोटा-सा उदाहरण आपके सामने और रखूंगा जो आपने 300 साल की न्यूटन वाली बात कही, बहुत ठीक कही; लेकिन पूरा विज्ञान वही समाज नहीं चलाता। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं जिन पर समाज टिकता है। केवल एक फल टपकने की बात जो हुई उससे एक बड़ी दिशा मिली। लेकिन और भी बहुत कुछ पीछे-पीछे चलता है। मैं पहाड़ियों पर खेती संबंधी एक उदाहरण आपके सामने रखंगा, जिसे सीढ़ीदार खेती कहते हैं, सारे पहाड़ों में दुनियाभर के पहाड़ों में, कोई ट्रान्सफर ऑफ टेकनॉलॉजी सेमिनार नहीं हुआ होगा। जहां भी जो आदमी था, किसान था, उसने देखा कि इन पहाड़ों में अगर दो मुट्ठी अनाज पैदा करना है तो सीढ़ियां बनानी पड़ेगी। आप क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, यकीन मानिए पूरी दुनिया की पर्वतमाला में सीढ़ीदार खेत के लिए जो आदर्श कोण होना चाहिए, ढाल का वही कोण मिलेगा। प्रयोग किए होंगे लोगों ने, 100-200 वर्ष प्रयोग में लगाए होंगे।
आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उसका जो स्लोप होता है वह बाहर की तरफ होता है। दुनिया में एक बड़ी संस्था है। कृषि संबंधी, संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले, विश्व खाद्य संगठन। इनके वैज्ञानिकों ने करीब 40 वर्ष तक टनों पेपर लिखे हैं कि सीढ़ीदार खेतों का स्लोप ‘आउटवर्ड' न होकर इनवर्ड' होना चाहिए वरना ‘मिट्टी का कटाव' होता है। मतलब यही कि दुनिया भरके किसान मूर्ख हैं और उन्होंने सारे सीढ़ीदार खेत गलत बनाए। यदि दुनिया भर के सीढ़ीदार खेतों की सीढ़ियों को ठीक करना हो तो यह असंभव बात है, सभी संस्थाओं को अन्य काम छोड़कर इसी के लिए लग जाना होगा। ‘आउटवर्ड' सारी दुनिया ने किया, लेकिन इतनी बड़ी गलती सभी ने कैसे की जबकि विश्व खाद्य संगठन चालीस वर्ष तक कहता रहा कि स्लोप ‘इनवर्ड' होना चाहिए। जहां-जहां उन्होंने ग्रान्ट देकर नए सीढ़ीदार खेत बनवाए वहां उन्होंने जोर दिया कि स्लोप ‘इनवर्ड' रहे। दस वर्ष के बाद नतीजे मिले तो पता चला कि जहां भी स्लोप भीतर की ओर है वहां जमीन में भूस्खलन ज्यादा हुए। तब उन्होंने पाया, जब सीढ़ीदार खेत का स्लोप पीछे की तरफ होता है, तो पानी वहीं जमा होकर नीचे जाता है और पृथ्वी को जल्दी काटता है। तो, वे सारे किसान जो हजारों वर्षों से बाहर की तरफ स्लोप बना रहे थे, गलत नहीं हैं। फिलहाल विश्व खाद्य संगठन ने अपनी गलती को स्वीकार किया है।
एक और छोटा-सा उदाहरण, घराट, यानी पानी से चलने वाली चक्की। सारे पहाड़ों में, दुनिया के किसी भी पहाड़ पर जाइए, वहां का बढ़ई, वहां का लुहार, पत्थर टांकने वाला सिलावट, इन तीन लोगों का सबसे अच्छा मिलना जो होता था, वह घराट बनाने में होता था। किसी समाज सेवक मित्र ने कहा कि यह घराट पुरानी पड़ गई है, इन पर काम आगे नहीं हुआ है, इनको सुधारा नहीं गया है। अगर वहां का हवा पानी नहीं बदला तो उस पत्थर का सुधार कैसे हो? तो भी, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट वगैरा किया और कुल 40,000 घराटों की उन्होंने सूची बनाई जिनमें से 40 को सुधारा गया। मेरा कहना है कि चालीस की धुरी में आप सोने की कील भी लगा। दीजिए या हीरे की। लेकिन 40,000 घराट जिस गति से, जिस ढंग से चलाने का जो कुल वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें हम लोगों को आस्था और भरोसा रखना चाहिए। और जैसा आपने बहुत ठीक कहा कि तीन सौ सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं, उनके बदलने की अपनी एक दिशा है - उसका यह एक अंश मात्र है।
आगे मैं एक-दो उदाहरण इस प्रांत मे संबंधित देना चाहूंगा। यहां का रायलसीमा, जिसे अकाल ग्रस्त इलाका माना गया। यहां पर दक्षिण में, हैदराबाद में, तालाबों की सबसे अच्छी परंपरा मिलेगी। वो लोग पागल नहीं थे कि इस इलाके में सबसे अधिक तालाब बनाए। यहां तालाबों की अधिक जरूरत थी। उसमें एक विशेष पद्धति का नाम है दशपला पद्धति। यह हम लोगों ने सीखा, आप लोगों से। दस तालाबों को एक-दूसरे से जोड़ना, कभी दस नहीं होंगे, नौ भी होंगे या ग्यारह भी हो सकते हैं। तो जहां पानी कम बरसता है, वहीं तालाबों के जल प्रबंध की सबसे व्यवस्थित योजनाएं बनी। और इन्हें किसी सिविल इंजीनियर ने नहीं, समाज के सभी सदस्यों ने बनाया था। तालाब कहां बनेगा, उसका कैचमेंट कहां, कितना होगा, अतिरिक्त पानी कहां से निकलेगा, ‘एप्रन' कैसा होगा आदि। और ये नाम आपको तेलुगू, तमिल, हिन्दी सब में मिलेंगे। एक है। वेस्ट वियर सिस्टम (स्पिलवे), जिससे तालाब का पानी निकलता है। चाहे बड़े से बड़ा बांध हो, हुसैन सागर हो या छोटा जलाशय हो, उसमें वेस्टवियर जरूर होता है। इसे हम लोगों की तरफ ‘अफरा' कहते हैं। यानी पेट अफर गया तो खाने से मना कर देते हैं। उसी प्रकार तालाब का पेट भर गया तो उसका पानी बाहर निकल जाता है। उसका एक नाम ‘नेष्टा' है जो संस्कृत के निशृष्य' से बना है - सांस छोड़ना या पानी छोड़ना तालाब से। ये ‘नेप्टा' शब्द जैसलमेर में भी चलता है और पाकिस्तान में भी, जिसे उर्दू का इलाका मानते हैं - एक मात्रा भी घिसी नहीं। तो लोगों का विज्ञान केवल भाषा से ही नहीं चलता है; जो उपयोग की चीजें होती हैं, उन्हें अच्छे ढंग से अपनाने में कहीं दिक्कत नहीं होती है।
यहां आकर मुझे एक और चीज़ आप लोगों से सीखने को मिली। वह यह है कि जब भाषा ज्ञान-विज्ञान के काम में इतने रमे रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोग बहुत सहजता से बताते गए कि यह हमें नहीं मालूम। ये कैसे काम करता है, सेल को संदेश कैसे मिलते हैं या मॉलिक्यूल को संदेश कैसे मिलते हैं?'' शायद उच्चारण मेरे गलत होंगे। कोशिका सिग्नल पर भी शोध चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने बताईं। एक तरफ से, हमें संसार का जितना ज्ञान है उससे कहीं अधिक संसार अज्ञात भी है। इसका ज्ञान होना भी बहुत बड़ा ज्ञान है कि हम लोगों को कितना नहीं पता? शायद आप लोग जानते होंगे कि ‘एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अननोन थिंग्स' भी तैयार हो रहा था। उसकी स्थिति क्या हुई मालूम नहीं। उसमें चैप्टर पर चैप्टर जुड़ते जा रहे थे उस समय। यहां आकर मालूम पड़ा कि कितना ज्ञात है उसी में से निकलता है। कि कितना अज्ञात भी है। इस सबसे मन में श्रद्धा का भाव उभरता है कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करें ज्ञान विज्ञान का। और इसमें नतमस्तक हों, एक शक्ति के प्रति, जिसे हम श्रद्धा से देखें। वह शक्ति समाज की हो सकती है, प्रकृति की हो सकती है, ईश्वर की हो सकती है।
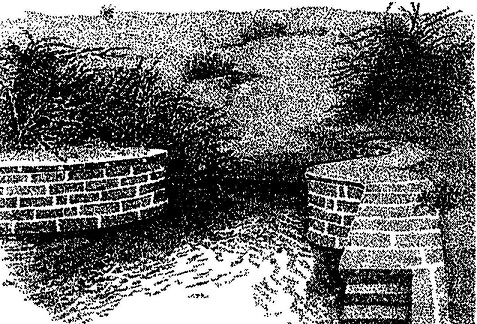
नेप्टाः यूं तो हरेक तालाब में अधिकतम कितना पानी भरा जाए इसकी कोई-न-कोई सीमा तय की जाती है। इस अधिकतम स्तर को पार करने के बाद पानी की निकासी के लिए नेष्टा बनाए जाते हैं। नेष्टा की वजह से तालाब की मेड़ टूटने का खतरा भी कम हो जाता है।
एक-दो चीजें जो छोटे-छोटे सवालों में से उठी। बायोडाइवर्सिटी, आप लोगों के लिए यह शब्द अपरिचित नहीं। भाषाओं के मामले में भी इस शब्द को भूलना नहीं चाहिए। मोनोकल्चर जितना धरती के लिए खराब है, फसल के लिए खराब है, उतना ही भाषा के लिए भी। अगर सारी दुनिया की भाषा एक हो जाएगी तो वह अच्छी बात नहीं होगी। बायोडाइवर्सिटी भाषा में भी उतनी ही जरूरी है। दूसरा, मन से यह हटा देना चाहिए कि भाषा और विज्ञान दो अविभाज्य चीजें हैं। मुझे लगता है यह सत्ता और विज्ञान है। जिसके हाथ में सत्ता रहती है वह समय के विज्ञान को एक तरह से नियंत्रित करता है। आज और कल में हम लोगों ने कई यंत्र देखे और कार्यक्रम देखे तो पता चला कि नीदरलैण्ड को अनुदान है, फ्रांस की सरकार का अनुदान है, यह यंत्र वहां से आया है। तो यह कोई अंग्रेज़ी भाषा में काम करने वाले देश से थोड़े ही आता है सारा। आप लोगों को अच्छा लगा तो, आप लोगों ने वहां से लिया। अगर उनके यहां किसी यंत्र की तरक्की हुई है तो अंग्रेजी के कारण नहीं हुई है, वहां उनकी अपनी भाषा के कारण हुई, अपनी मेहनत के कारण हुई है।
मैं ऐसा मानता हूं कि जहां अंग्रेजी बोली जाती है वहां तरक्की हुई तो अंग्रेज़ी के कारण नहीं बल्कि उनकी अपनी भाषा के कारण हुई है। तो जोर अंग्रेजी पर न रख कर अपनी भाषा पर रखना चाहिए। कुछ चीजें शायद ऐसी हो सकती हैं। जो ‘तुम्हीं ने दर्द दिया तुम्हीं दवा देना। अगर दर्द उनका है तो कई बार दवा भी उनकी ही लेनी पड़ती है। आपको रॉकेट ही बनाना है तो रॉकेट की टेकनॉलॉजी उसी भाषा से लेनी होगी। उसमें यदि संस्कृत के शब्द अनुवाद करके ले आऊं या मैं बोलूं कि मैं बोलियों से शब्द ले आऊंगा, यह संभव नहीं होगा। नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे। तो दर्द उनका है तो दवा भी उनकी लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम अपने को, अपने समाज को फिर से नये सिरे से देख सकें। जो उसके दर्द हैं उसके लिए हम दवा, उसकी दवा, उसकी भाषा द्वारा दे सकें। उस पूरे समाज की लंबी यात्रा में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, जिसमें कुछ बाहर का दर्द हो और बाहर की दवा। पर सारी-की-सारी बाहर की दवा, बाहर की भाषा नहीं होगी। थोड़ी बहुत हर्बल की भी गुंजाइश होती है, आयुर्वेद की भी गुंजाइश होती है। आपके यहां यह काम अब शुरू हुआ है, बहुत पहले से ही कई संस्थाओं को इसमें काम करना था। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं तीन दिन में हमको अज्ञात संसार की यात्रा कराने के लिए।
नागयष्टिः अक्सर तालाबों में जलस्तर नापने के लिए कलात्मक स्तंभों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें नागयष्टि कहते हैं।
अनुपम मिश्र: राजस्थान में पानी के स्रोतों पर महत्वपूर्ण काम किया है। राजस्थान की रजत बूंदें' और 'आज भी खरे हैं तालाब' किताबों के लेखक हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली से जुड़े हैं। यह लेख विज्ञान साहित्य समागम से साभार। सभी चित्रः ‘आज भी खरे हैं तालाब' से।
यह लेख कोशिकीय एवं आण्विक जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अनुपम मिश्र द्वारा दिए गए व्याख्यान पर आधारित है। इस कार्यक्रम में भागीदार लेखकों, वैज्ञानिकों के विचारों को विज्ञान, साहित्य समागम' पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है।

