विज्ञान को आम तौर पर तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित सत्य की खोज माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर आंकड़े एक ही हों लेकिन अलग-अलग वैज्ञानिक भिन्न नतीजों तक पहुंचें? बीएमसी बायोलॉजी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है - एक ही डैटा सेट का विश्लेषण करते हुए भी वैज्ञानिक अलग-अलग परिणाम पा सकते हैं। यह अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि वे विश्लेषण के दौरान पद्धति को लेकर क्या निर्णय लेते हैं और किन आंकड़ों को नज़रअंदाज़ करते हैं।
यह अध्ययन पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इससे स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में लिए गए कुछ व्यक्तिगत निर्णय नतीजों में अंतर पैदा कर सकते हैं।
मेलबर्न विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र एलियट गोल्ड के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में 246 पारिस्थितिकीविदों की 174 टीमों को दो समान डैटा सेट देकर विश्लेषण करने को कहा गया था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत निर्णयों का अंतिम निष्कर्षों पर कितना प्रभाव पड़ता है।
प्रकरण 1: पहला सवाल यह था कि क्या घोंसले में चूज़ों के बीच प्रतिस्पर्धा का उनके विकास पर असर पड़ता है। सवाल ब्लू-टिट पक्षी के चूज़ों के संदर्भ में था। इस सवाल के विश्लेषण के लिए सभी समूहों को 452 पक्षी घोंसलों से सम्बंधित एक ही डैटा दिया गया था। लेकिन समूहों के परिणाम काफी अलग-अलग रहे:
● 5 टीमों ने सहोदरों की संख्या का विकास से कोई सम्बंध नहीं पाया।
● 5 टीमों के निष्कर्ष मिश्रित थे।
● 64 टीमों ने पाया कि अधिक सहोदरों की उपस्थिति से चूज़े धीमे बढ़ते हैं, लेकिन प्रभाव की निश्चितता और परिमाण को लेकर सहमति नहीं थी।
प्रकरण 2: दूसरा सवाल यह था कि क्या आसपास कम या अधिक घास होने से यूकेलिप्टस के पौधों के बचने-बढ़ने की संभावना प्रभावित होती है। इसके विश्लेषण के लिए डैटा ऑस्ट्रेलिया के उन 18 स्थानों से लिया गया था, जो यूकेलिप्टस के पुनर्स्थापन के काम में भाग ले रहे थे। यहां भी परिणाम विरोधाभासी थे:
● 18 टीमों ने पाया कि ज़्यादा घास हो तो पौधों के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है।
● 6 टीमों ने पाया कि ज़्यादा घास होने से पौधों को फायदा होता है।
● 31 टीमों ने निष्कर्ष दिया कि घास की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो सवाल है कि वैज्ञानिकों के निष्कर्ष इतने अलग-अलग क्यों थे? इसका कारण एक ही डैटा सेट का विश्लेषण करते समय वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग निर्णय लेना है। इसमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक:
▪ कौन-सी सांख्यिकीय विधि अपना रहे हैं?
▪ किन कारकों को नियंत्रित कर रहे हैं?
▪ अनुपलब्ध डैटा से कैसे निपट रहे हैं?
निर्णय लेने में शामिल विधियों में थोड़ा भी फर्क अंतिम निष्कर्ष में बड़ा अंतर ला सकता है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विज्ञान पूरी तरह वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि विश्लेषण के तरीकों पर निर्भर करता है।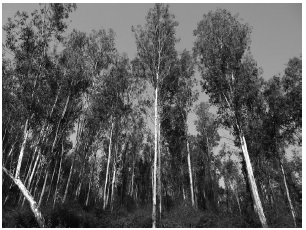
गौरतलब है कि यह समस्या केवल पारिस्थितिकी तक सीमित नहीं है। मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में भी ऐसे अलग-अलग निष्कर्ष निकल सकते हैं।
कुछ विशेषज्ञ, इसे वैज्ञानिक विश्वसनीयता के लिए गंभीर समस्या मानते हैं। अगर परिणाम इस पर निर्भर करते हैं कि डैटा का विश्लेषण कौन कर रहा है, तो क्या निष्कर्षों पर भरोसा किया जा सकता है?
वहीं, कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इन अध्ययनों में वैज्ञानिकों से ऐसे डैटा का विश्लेषण करवाया गया, जो उनके विशेषज्ञता क्षेत्र से बाहर थे। उदाहरण के लिए, ब्लू टिट पक्षियों पर शोध करने वाले वैज्ञानिक सामान्य पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों की तुलना में बेहतर सांख्यिकीय विधियां चुन सकते हैं।
सौभाग्य से, यह स्थिति सुधारी जा सकती है। वैज्ञानिक निम्नलिखित तरीकों से निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं:
o अधिक स्पष्ट प्रश्न पूछकर
o विश्लेषण के तरीके मानकीकृत करके
o डैटा विश्लेषण का बेहतर प्रशिक्षण देकर
इस अध्ययन का यह मतलब नहीं कि विज्ञान विफल हो रहा है। बल्कि, यह दर्शाता है कि डैटा विश्लेषण उतना सीधा-सरल नहीं होता, जितना हम सोचते हैं। इस समस्या को स्वीकार करना वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और भरोसेमंद बना सकता है।
तो, अगली बार जब आप किसी अध्ययन का बड़ा दावा देखें तो याद रखें कि इन फैसलों को देने वाला आखिर है तो इंसान, और हर इंसान थोड़ी जुदा सोच और समझ रख सकता है। नतीजतन, इसके अलग परिणाम भी हो सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)
-
Srote - June 2025
- भारत में दवाइयां इतनी महंगी क्यों? - भाग 1
- भारत में दवाइयां इतनी महंगी क्यों? - भाग 2
- कटहल के स्वास्थ्य लाभ
- बुलढाणा में फैली गंजेपन की समस्या
- कमला सोहोनी एक वैज्ञानिक महिला
- आंकड़े वही निष्कर्ष अनेक
- एक्सपांशन माइक्रोस्कोपी: सूक्ष्म अवलोकन के लिए जुगाड़
- समुद्र की अतल गहराइयों में छिपी अद्भुत दुनिया
- चट्टानों में हवा के बुलबुलों में छिपा पृथ्वी का अतीत
- पृथ्वी के घूर्णन से बिजली
- चंद्रमा की उम्र लगभग पृथ्वी के बराबर है!
- अत्तिला के हूण आखिर कौन थे?
- हड्डी के औज़ारों का इस्तेमाल कब शुरू हुआ?
- मकड़ियों की पतली कमर
- हमारी जोखिमग्रस्त डॉल्फिन की गणना
- पालतू और जंगली परागणकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा
- क्या सिंधु नदी का पानी रोक पाना संभव और उचित है?
- डॉ. संघमित्रा गाडेकर नहीं रहीं

